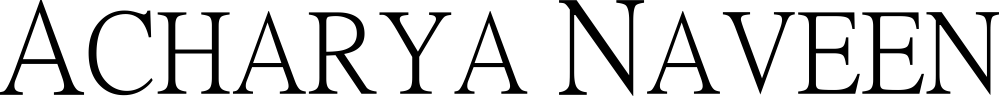मैं ना तो कोई महात्मा हूँ और ना गुरु। मैं अपने अमर अस्तित्व का खोजी हूं। मैं अपने भीतर के उस तत्व की खोज में हूँ जिस पर समय और स्थान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और यह तत्व अद्भुत रूप से हम सबके भीतर एक जैसा ही है क्योंकि हम सबका मूल स्रोत एक ही है। मैं इस मार्ग पर चलने वाला पहला व्यक्ति नहीं हूँ और ना ही अंतिम हूँ। मेरा मानना है कि सत्य ना तो नया होता है और ना ही अलग। सत्य तो शाश्वत होता है क्योंकि जो नया है वह पुराना हो जाएगा और जो अलग होता है वह सार्वभौमिक नहीं हो सकता। मानव जाति की हर पीढ़ी में परम सत्य को जानने वाले व्यक्ति हुए हैं और हमेशा होते रहेंगे।
दस वर्ष की उम्र में एक सूर्यास्त ने मेरी जीवनधारा को अध्यात्म की ओर मोड़ दिया। पिट्ठू फोड़ खेल खेलते हुए गेंद अचानक घर की छत पर चली गई थी। मैं उसे लेने के लिए छत पर गया था। जैसे ही मैंने गेंद उठाई और सामने देखा तो मैं एकदम ठहर गया। ऐसा लगा मानो इस दुनिया में मेरे अलावा कोई भी नहीं है। मैं बिल्कुल अकेला हूं। सबकुछ गायब हो गया। नीचे से मेरे साथी ने आवाज लगाई सुनता नहीं क्या….गेंद नीचे फेंक। आवाज सुनकर मैं नीचे आ गया। छत पर जो मैंने देखा वह था –सूर्यास्त। डूबते हुए सूरज ने मुझे भी अकेलेपन की अनंत गहराइयों में डूबा दिया। हालांकि मेरे माता-पिता, भाई-बहन सब थे, फिर भी मुझे अकेलेपन का गहरा एहसास हुआ। इस दृश्य का मेरे अंतर्मन पर एक स्थायी असर पड़ा और यह अकेलापन हर वक्त मेरे साथ रहने लगा। कुछ ही दिनों के बाद घटी दूसरी घटना ने मेरे अकेलेपन को जिज्ञासा में बदल दिया। यह घटना थी शवयात्रा के दर्शन। हमारा घर एक ऐसे मार्ग पर था जिसके दक्षिणी छोर पर श्मशान घाट था। हमारे घर का मुख पूर्व की तरफ था। घर के बाहर खेलते हुए अचानक मेरी नजर वहां से गुजरती एक शवयात्रा पर पड़ी और मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मेरे भीतर एक सिहरन सी दौड़ गई। मैं नहीं जानता कि क्या हुआ? शायद एक डर बैठ गया। अतः बार-बार मेरे मन में ये विचार आने लगे कि-
मृत्यु क्या है?
क्या मृत्यु के बाद जीवन है?
शायद नहीं है ……. लेकिन यदि हुआ तो!
इस घटना ने मुझे मृत्यु के रहस्य को जानने के लिए प्रेरित कर दिया। ये दोनों घटनाक्रम मेरे अंतर की गहराइयों में उतर गए और एक मंथन मेरे अंतर्मन में हर वक़्त चलने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं यह मानने को तैयार नहीं था कि मनुष्य की रचना समय और स्थान की घाटी में भटकते रहने के लिए हुई है। मैं सब काम करता था- खाना-पीना, खेलना-कूदना, पढना-लिखना; लेकिन मेरे अन्दर हमेशा एक अग्नि सुलगती रहती थी कि जीवन जीने के दो मार्ग है– एक वो जिसका अंत कभी भी हो सकता है और दूसरा वो जिसका कोई अंत नहीं, जो अनंत है। मुझे किस पर चलना चाहिए? इस प्रकार लगातार दो वर्ष मंथन करने की उपरांत मैंने यह दृढ निश्चय कर लिया कि मैं उस राह पर नहीं चलूँगा जिस पर चलने के कुछ समय बाद हार माननी पड़े और इस तरह मैंने शाश्वत जीवन के मार्ग पर चलने का संकल्प कर लिया ।
12 वर्ष की उम्र में मैंने अपने पिता को इस निर्णय से अवगत करवा दिया। उन्होंने मेरा विरोध किया लेकिन मैंने उनकी असुरक्षा के भाव को दूर किया कि मैं घर छोड़ कर कही नहीं जाऊंगा और अपनी सभी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाऊंगा। क्योंकि मैं ये जान चुका था कि अध्यात्मिक उत्थान के लिए त्याग की नहीं वैराग्य की जरूरत है। फिर वो सहज हो गये। धीरे धीरे उन्हें मेरी लगन की दृढ़ता का अहसास हो गया।
अपनी किशोरावस्था के प्रथम वर्ष से मैंने स्वाध्याय और ध्यान शुरू कर दिया। मेरे नानाजी से मुझे ध्यान करने की प्रेरणा मिली। मेरी जिज्ञासा को देखते हुए 14 वर्ष की आयु में 2दिसम्बर 1993 को मुझे ट्यूशन पढ़ाने वाले अध्यापक ने जिला पुस्तकालय का सदस्य बनवा दिया। उसके बाद तो मेरे स्वाध्याय को जैसे पंख लग गए। इतिहास और दर्शन मेरे प्रिय विषय रहे है। मैंने दोनों को एक साथ पढ़ने का प्रयास किया ताकि मैं महापुरुषों के विचारों को सही सन्दर्भ में समझ सकू। इसी कारण मैं इतिहास के अध्यात्मिक प्रवाह को समझ पाया। उस परम सत्ता को पाने के सही मार्ग को जानने के लिए मैंने संसार के सभी दार्शनिको को पढ़ा और धीरे-धीरे रात्री के अन्धकार में सितारों की तरह सार्वभौमिक मार्ग की पगडण्डी चमकने लगी। तेज रफ़्तार की बजाय सही दिशा मेरे लिए अधिक महत्वपूर्ण थी। मैं जानता था की सभी साधन चंद्रमा पर नहीं पहुचते । स्वाध्याय के साथ-साथ मैं नियमित रूप से ध्यान भी करता था क्योंकि मुझे लगता था कि यह विषय बुद्धि और इन्द्रिओं की सीमा से परे है । इसका अर्थ ये नहीं है की बुद्धि का महत्व नहीं है, जरूर है लेकिन उतना ही जितना पानी में स्विम शूट का होता है, उसके बाहर वह सिर्फ एक बोझ है।
ध्यान के द्वारा मेरी संवेदनशीलता का विस्तार हो चुका था। हर रक्त के साथ मैं अपना अटूट संबंध महसूस करता था। लिंग, जाती, धर्म और देश के सभी बंधन टूट चुके थे। अपने आसपास के किसी भी प्राणी को दुखी देखने पर मेरा मन प्राय दुखी हो जाता। सबकी पीड़ा मुझे अपनी सी लगती थी। मुझे लगता था कि आनंद और ज्ञान पर सबका जन्मसिद्ध अधिकार है।
मेरी सबसे पहली शिक्षक प्रकृति ही थी और इसमें मेरी भूमिका एक दर्शक की थी। लेकिन मेरे देखने में एक जागृति थी। रात्रि के आकाश को निहारना मुझे बहुत अच्छा लगता था। सात तारों से बना प्रश्नवाचक चिन्ह देखकर लगता था कि यह ब्रह्माण्ड मुझसे सात प्रश्न पूछ रहा है जिनका हल खोजने के लिए हमें संसार में भेजा गया है। मृत्यु जीवन का अंत है या आरम्भ, यह तो मेरी प्रथम जिज्ञासा थी ही लेकिन धीरे धीरे इसी से जुड़े हुए कुछ और प्रश्न भी मेरे अंतर्मन में प्रकट होने लगे। वे प्रश्न इस प्रकार हैः-
1. हम कौन है?
2. हम कहां से आए है?
3. हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है?
4. उस लक्ष्य की प्राप्ति कैसे हो?
5. मृत्यु जीवन का अन्त है या आरम्भ?
6. सत्य क्या है-जो दिखाई देता है वह या जो अदृश्य है वह?
7. ऐसा क्या है जिसे प्राप्त करने के बाद और कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता?
मुझे लगता है ये सात शाश्वत प्रश्न है। मेरा सम्पूर्ण जीवन इन्हें हल करने को समर्पित है। मैं हमेशा सोचता था कि आखिर क्या है मनुष्य जीवन का मकसद? मैं कौन हूँ , क्या इस शरीर से हट कर भी मेरी सत्ता है? क्या इस नश्वर शरीर की देखभाल करते रहना ही जीवन का लक्ष्य है, या फिर कभी ना तृप्त होने वाले मन की इच्छाओं को पूरा करने में लगे रहना ही इस जीवन का लक्ष्य है। यदि ऐसा है तो इस लक्ष्य को इस पृथ्वी पर आज तक कोई भी पूरा नहीं कर पाया है। आज तक कोई भी अपने शरीर को बुढापे व मृत्यु से नहीं बचा पाया है और ना ही कोई इंद्रियों के स्तर पर अपने मन को संतुष्ट कर पाया है। निस्संदेह जीवन का लक्ष्य सुख प्राप्ति है, लेकिन कैसा सुख, जो आज है कल नहीं। वह जिसे पाने से पहले पाने की तृष्णा व पाने के बाद खोने का भय लगा रहता है। जिसे न तो पाने से पहले तृप्ति होती है, न पाने के बाद। इतिहास इस बात का साक्षी है।
इस तरह मेरी सारी किशोरावस्था निरंतर स्वाध्याय और ध्यान में बीती। आखिर अपनी युवावस्था के प्रथम वर्ष (20वें में) मुझे पहला आध्यात्मिक अनुभव हुआ और मैं जान पाया कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं है। मेरी ख़ुशी और आनंद का ठिकाना न रहा। इस अनुभव के ठीक 3 महीने बाद 29 अगस्त 1999 को मेरी मुलाकात स्वामी रामकृष्ण परमहंस सरीखे ही एक महात्मा से हुई। उनका नाम श्रीराम दुबे था। मैं बीकानेर अपने मौसा जी के घर गया हुआ था। उनके घर में श्रीराम दुबेजी आए और पहली ही मुलाकात में उन्होंने मुझे कहा मैं तुम्हें पिछले तीन जन्मों से जानता हूँ। फिर उन्होंने मेरे पिछले जन्मों के विषय में बताया। उनके अनुसार मनुष्य शरीर में मुझे लगातार 321 वर्ष हो चुके हैं और यह मेरा अंतिम जन्म है। मुझे नहीं पता यह कितना सत्य है लेकिन हां 12 वर्ष की आयु से मुझे जो शब्द सबसे अधिक प्रिय है वह है- मोक्ष। मुझे लगता है कि हम सब यही चाहते हैं। लेकिन हमे अपनी इस चाहत के सही रूप का अहसास नहीं है। आखिर दुखो से मोक्ष कौन नहीं चाहता है। मुक्ति का यह रूप सबकी चाहत है। मेरे ख्याल से मृत्यु की मृत्यु अथवा जीवन का जीवन ही मोक्ष है। 7 वर्ष मुझे श्री राम दुबे जी का दिव्य सानिध्य मिला। उसके पश्चात एक और महात्मा के सुपुर्द करके वे इस संसार से चले गए।
अपने अनुभव के आधार पर मैं यह कह सकता हूँ कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं है। ध्यान के जरियें आप भी इस सत्य का अनुभव कर सकते है । जागो मेरे साथियों, और खोज करो उसकी जो आपके भीतर है, जो आपका अपना है, जिस से बढ़कर कुछ नहीं और जो कभी नष्ट नहीं होता। यदि आप विज्ञान के द्वारा इस सत्य की प्रमाणिकता का इंतजार करना चाहते है तो आपकी मर्जी है। इस सदी के मध्य तक यह भी प्रमाणित हो जायेगा। मेरा मानना है कि विज्ञान अध्यात्म का जाना जा चुका हिस्सा है और अध्यात्म विज्ञान का अज्ञात हिस्सा है । लेकिन निर्णय लेने से पहले मेरी एक बात का जवाब दे दीजिये– यदि आप कोपरनिकस से पहले पैदा हुए होते तो क्या हेलिओ सेंट्रिक थ्योरी का विरोध कर रहे होते या फिर राईट बंधुओ से पहले पैदा हुए होते तो उड़ने के सिद्धांत का विरोध कर रहे होते। क्या यह सही दृष्टिकोण होता जीवन जीने का।
एक बार विज्ञान की एक पुस्तक में मैंने पढ़ा कि एक मामूली से पौधे का खिंचाव भी प्रकाश की ओर होता है। यदि हम एक पौधे को एक ऐसे गत्ते के डिब्बे से ढक दें, जिसके एक तरफ से अंदर प्रकाश जाने के लिए छेद हो तो कुछ दिनों बाद गत्ता हटाने पर हम पाएंगे कि उस पौधे का झुकाव रोशनी की तरफ ही था। मैंने महसूस किया कि जब एक छोटे से पौधे में भी प्रकाश को पाने की ललक होती है तो फिर मुझे ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। मुझे लगा कि दुनिया की सभी जीवात्माएं जन्म जन्मांतर से प्रकाश की खोज में है तथा पौधे से लेकर आज तक हम जिस प्रकाश की तलाश में है वह पूरी होने का समय अब आ गया है। यह मनुष्य जीवन ही इस यात्रा का अंतिम पड़ाव है।
हम सब आनंद की दौड़ के धावक हैं लेकिन हम में से किसी को भी यह नहीं पता की इस दौड़ का विजेता वह होता है जो दौड़ना बंद कर देता है। ठहराव ही जीवन का लक्ष्य है और ठहराव आनंद में है अर्थात ठहराव ही आनंद है। जो कुछ भी है हमारे भीतर है और इसे पाने के लिए हमे कुछ नहीं करना है। जी हाँ, हर रोज़ कुछ भी न करने का अभ्यास करना है। इस कुछ भी ना करने का मतलब है- ध्यान। तन और मन की पूर्ण निश्चलता ही ध्यान है। इस यात्रा की सबसे अद्भुत बात यह है कि इसकी शुरुआत भी खुद से होती है और अंत भी खुद पर होता है। समय के मुसाफिर भी हम हैं और मंजिल भी हम ही हैं।